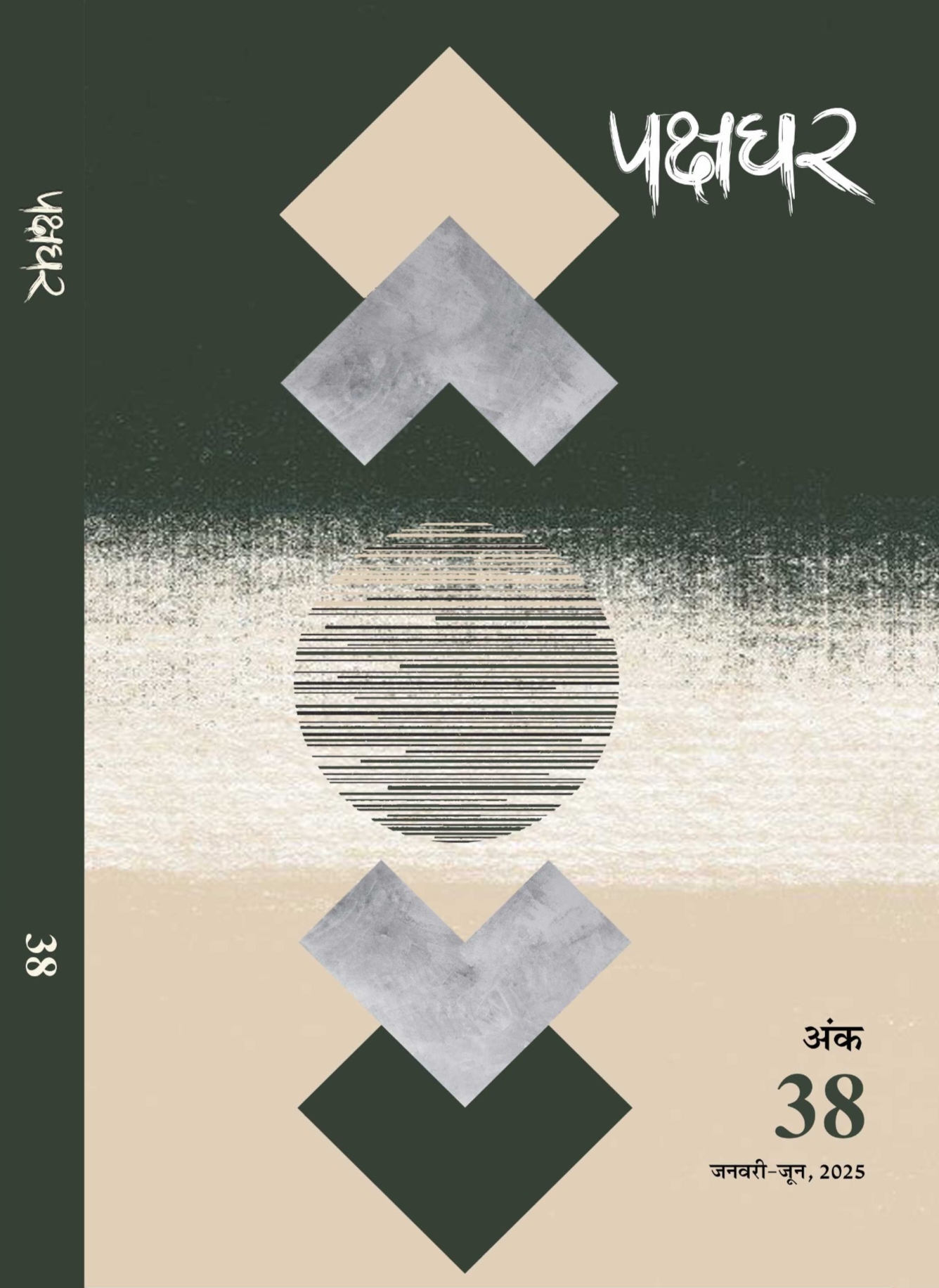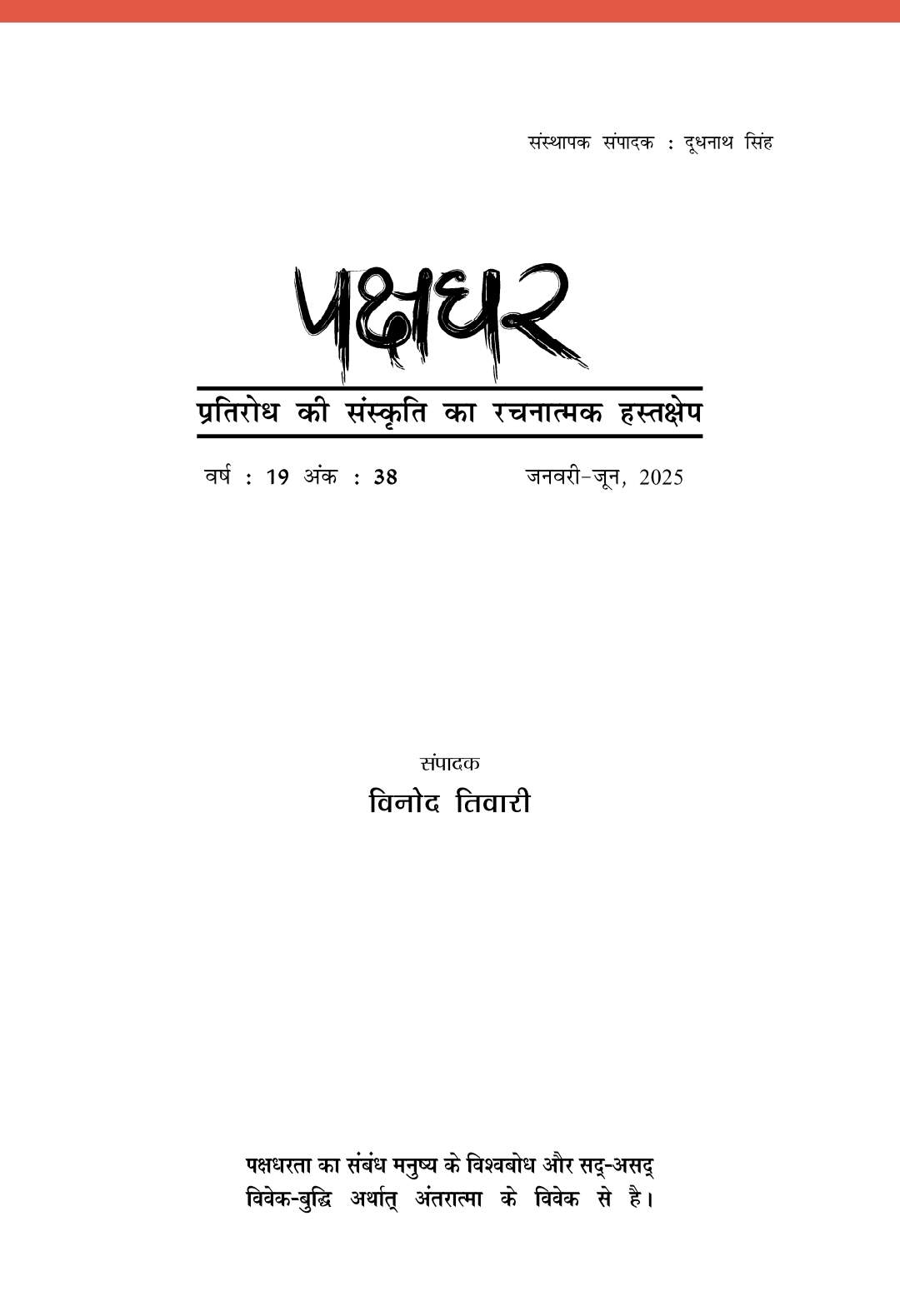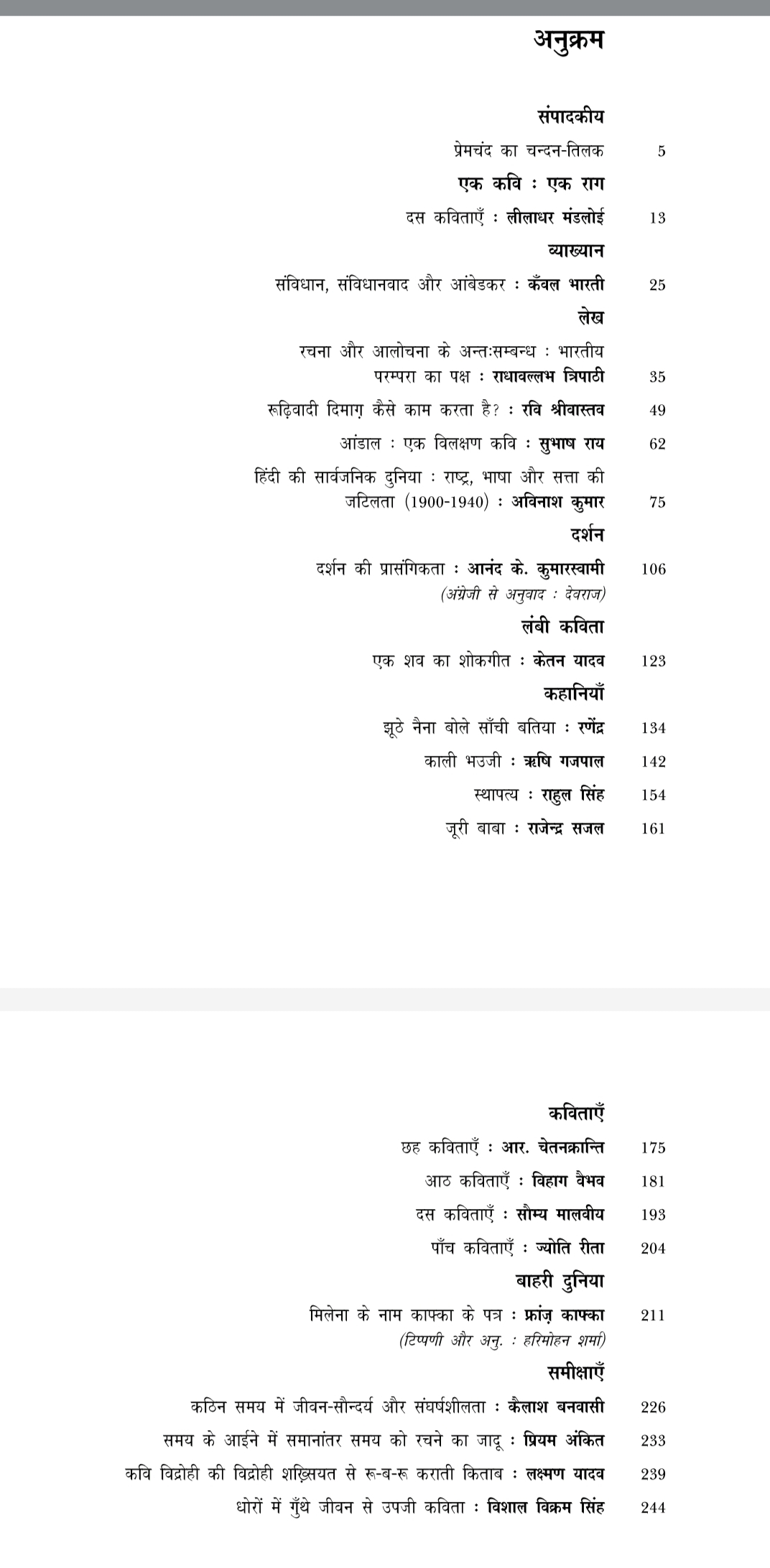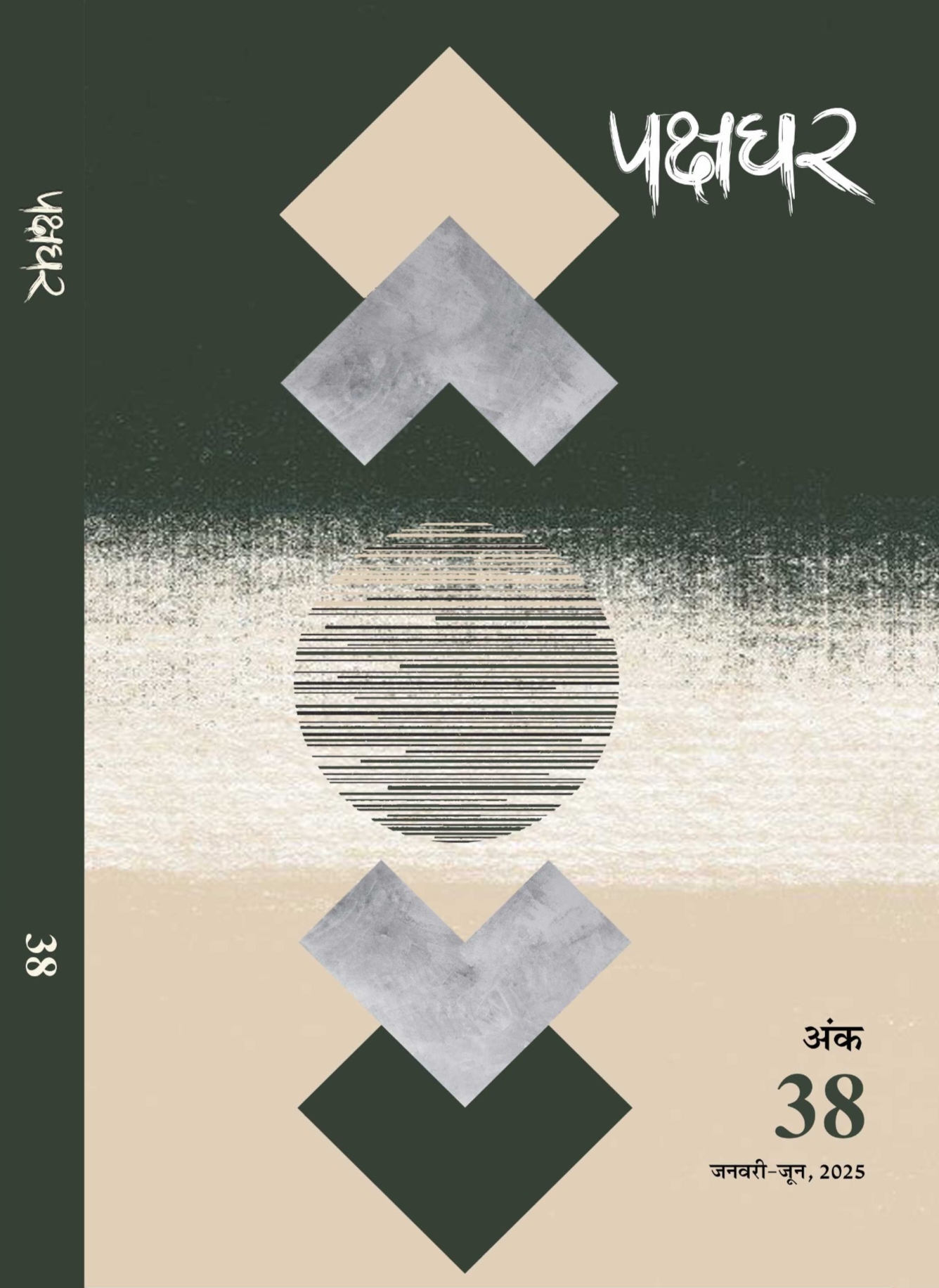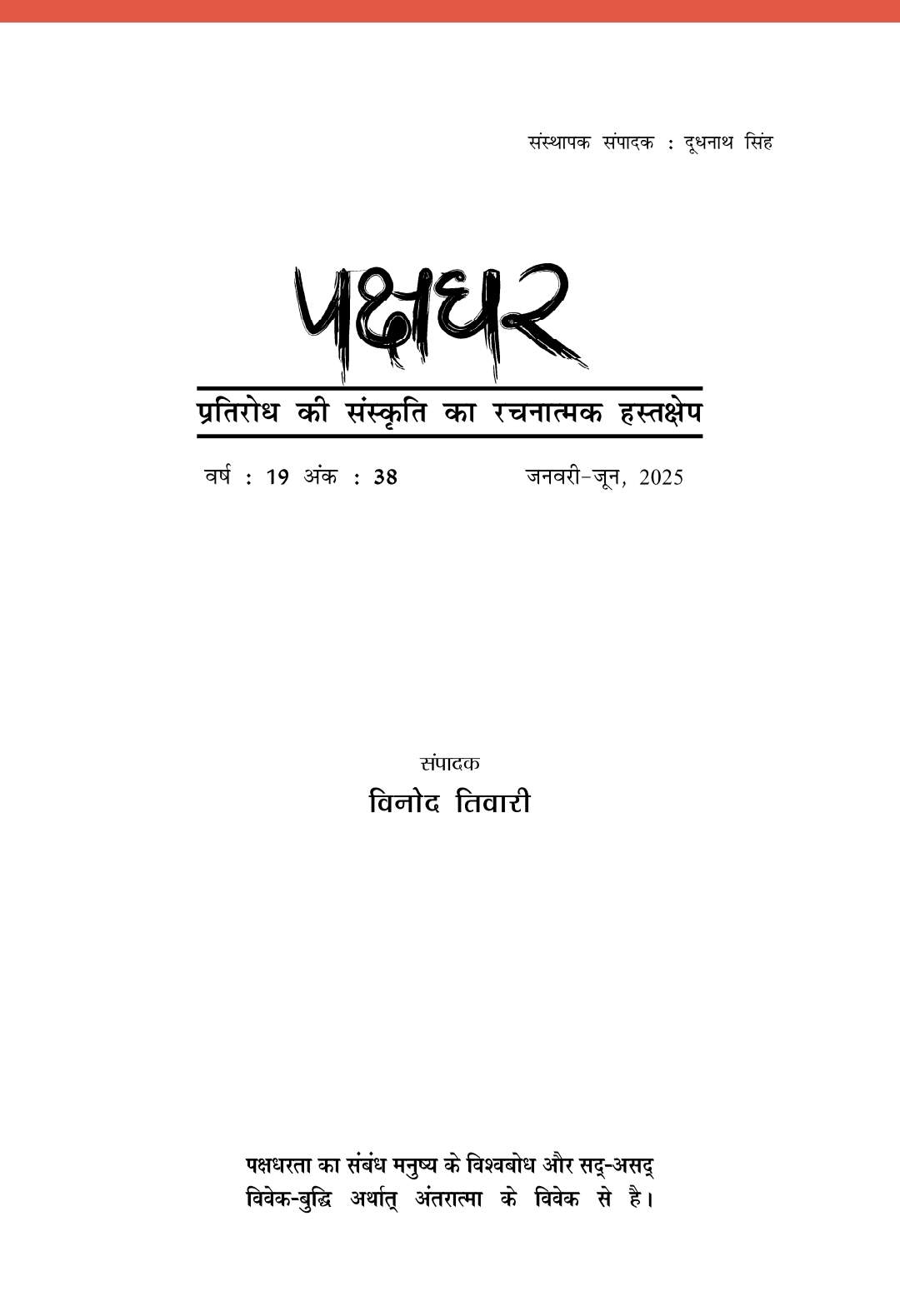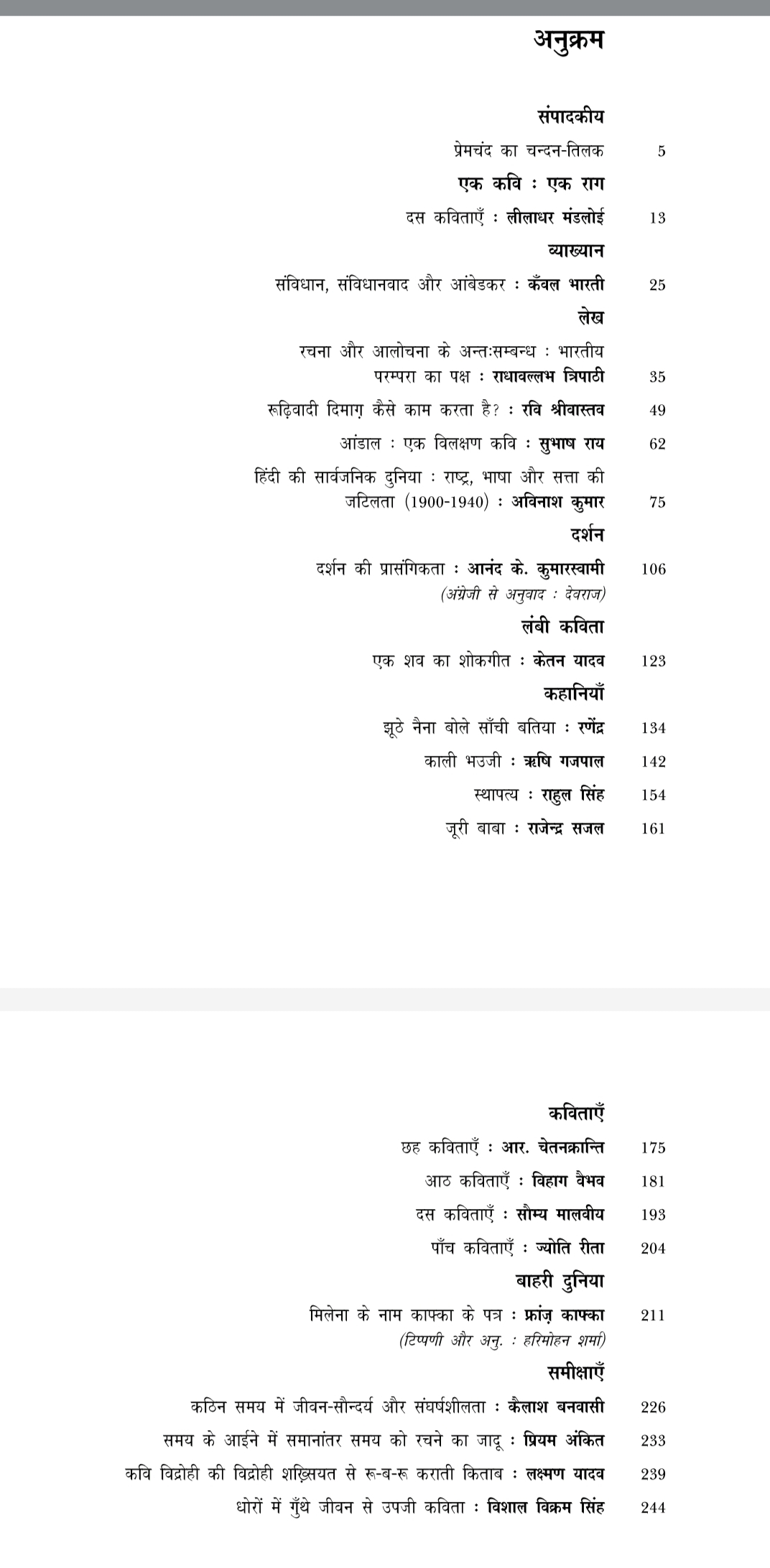ताज़ातर
पक्षधर_38
संपादकीय
प्रेमचंद का चन्दन-तिलक
दो-ढाई दशक पूर्व प्रेमचंद को दलित विरोधी और ब्राह्मणवाद का समर्थक लेखक कहने और
उनका विरोध करने वाले दलित लेखकों का एक समूह हुआ करता था, उनमें से कुछ लोग
आज भी यदा-कदा ज़ोर मारते रहते हैं । अब इधर एक नयी प्रवृत्ति देखने में आई है कि एक
ख़ास काट के ‘संस्कृतिवाद’ के पोषक और प्रचारक अपने ब्राह्मणवादी-पुरोहितवादी एजेंडे के
भीतर प्रेमचंद के समाहितीकरण का यज्ञकर्म कर रहे हैं । देखा जाए तो उक्त दोनों में बहुत
फ़र्क़ नहीं है । एक वर्ग जहाँ हवन और दहन में विश्वास करता है, तो दूसरा यज्ञ और
शुद्धिकरण में । पर, इनके ऋत्विक और यजमान यकसां हैं । परिप्रेक्ष्य भी यकसां कि प्रेमचंद
ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, हाँ उद्देश्य भले ही जुदा-जुदा हैं । पर, प्रेमचंद हैं कि अपने लेखन के
बल पर बार-बार, हर बार इस तरह के प्रपंच को मुँह बिराकर, उसी ज़मीन पर खड़े मिलते
हैं, जिस पर वह 1936 में दृढ़ता के साथ खड़े थे – गोदान, कफ़न, साहित्य का उद्देश्य और
महाजनी सभ्यता की पुख्ता ज़मीन पर । इस ज़मीन का आरंभिक छोर 1905 के आसपास
जाता है । वहाँ से लेकर 1936 तक प्रेमचंद ने 30-31सालों का सफ़र तय किया । जाहिर है,
इस सफ़र में एकाधिक मोड़ देखने को मिलते हैं, पर पड़ाव ही के रूप में, गंतव्य उनका
समाजवादी मानववाद ही था । वह ‘एकात्म मानववाद’ बिल्कुल नहीं था, जिसकी पूजा और
जिसका गुणगान उपर्युक्त ‘संस्कृतिवादी’ दल और विचार के लोग करते हैं । पंडित दीनदयाल
उपाध्याय का ‘एकात्म मानववाद’ धर्म को निजी आस्था के विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक
सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखता है । भारतीय संविधान में जहाँ जनता की ताक़त
(भारत के लोग) को संप्रभु माना गया है, वहीं ‘एकात्म मानववाद’ में धर्म को वह संप्रभुता
प्रदान की गयी है । इसलिए सीधे तौर पर न सही, किन्तु परोक्ष रूप से यह सिद्धान्त
धर्मराज्य का समर्थन करने वाला सिद्धान्त है । मार्च, 1933 का प्रेमचंद का एक भाषण है –
‘साहित्य की प्रगति’ । उस भाषण में प्रेमचंद कहते हैं कि “ईश्वर का ज़िक्र बड़े मौके से आ
गया । साहित्य की नवीन प्रगति उनसे विमुख हो रही है । ईश्वर के नाम पर उनके उपासकों
ने भू-मण्डल पर जो अनर्थ किए हैं, कर रहे हैं, उनके देखते इस विद्रोह को बहुत पहले उठ
खड़ा होना चाहिए था । आदमियों को रहने के लिए शहरों में स्थान नहीं, मगर ईश्वर और
उनके मित्रों और कर्मचारियों के लिए बड़े-बड़े मंदिर चाहिए । आदमी भूखों मर रहे हैं, मगर
ईश्वर अच्छे से अच्छा खाएगा, अच्छे से अच्छा पहनेगा और खूब विहार करेगा ।” अपने एक
अन्य भाषण – ‘जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान’ (जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के
बिहारी एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव पर दिया गया था) में कहते हैं, “मेरा ख़्याल है कि
समाज में जितनी अनीति है, उनमें सबसे घृणित धार्मिक पाखंड और धूर्तता है ।”
अतः जो लोग बेसिर-पैर की बातों के जरिये अनंत प्रलाप करने और भ्रामक वितंडा के
प्रचार-प्रसार में लगे हैं, उन्हें इस फ़र्क़ को समझ लेना चाहिए । जो लोग, आरंभिक दौर में
प्रेमचंद के आर्यसमाजी होने को हिन्दू धर्म के प्रचारक की तरह प्रस्तुत करते हैं, वह भूल जाते
हैं कि भगत सिंह का परिवार भी आर्य समाजी था । राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ आर्य समाजी थे
। भगत सिंह पर उनके आरंभिक दिनों में हो सकता है कि आर्य समाज का कुछ असर रहा हो
पर उससे क्या सिद्ध होता है ? जिस आदमी ने ‘मैं नास्तिक क्यों हूँ’ जैसा लेख लिख कर धर्म
और उसके पाखंड को पोषित और संरक्षित करने के लिए बनाए गए सिद्धांतों की आलोचना
करते हुए यह घोषित किया कि “मेरे प्रिय दोस्तो! ये सिद्धान्त विशेषाधिकार युक्त लोगों के
आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूँजी तथा उच्चता को इन सिद्धान्तों के आधार
पर सही ठहराते हैं। अपटान सिंक्लेयर ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास
दिला दो और उसके बाद उसकी सारी सम्पत्ति लूट लो। वह बगैर बड़बड़ाये इस कार्य में
तुम्हारी सहायता करेगा । धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबन्धन से ही जेल,
फाँसी, कोड़े आदि के सिद्धान्त उपजते हैं । प्रेमचंद ने तो साफ़ तौर पर धर्म पर चुटीला व्यंग्य
करते हुए लिखा कि ‘आजमाए हुए को आजमाना मूर्खता है ।’ इसलिए, उनका प्रगतिशील
लेखक संघ के 1936 की सदारत के बाद लाहौर आर्यभाषा सम्मेलन में अध्यक्षता के लिए
जाने को जिस तरह से पेश किया जाता है, उससे क्या सिद्ध होता है कि प्रेमचंद पक्के
आर्यसमाजी थे ? 1 अप्रैल 1936 को ज़माना के संपादक दया नारायण निगम को लिखे पत्र
में प्रेमचंद लिखते हैं – “भाईजान, तसलीम । मैंने तो इधर तीन माह से एक अफ़साना भी
नहीं लिखा । बस जामिया में ‘कफ़न’ लिखा था । इसके बाद लिखने की नौबत न आयी । हाँ,
यार इन सदारतों के मारे परेशान हूँ । मैंने मिस्टर सज्जाद ज़हीर से बहुतेरा कहा भइ, मुआफ़
करो, मुझे अपना काम करने दो । मगर न माने । 10 को लखनऊ और वहाँ से लाहौर । वहाँ
आर्य समाज की जुबिली के साथ एक आर्यभाषा सम्मेलन हो रहा है । वहाँ 11 को मुझे
सम्मेलन का सदर बनना है और वहाँ जाऊंगा तो चार-पाँच दिन लग ही जाएंगे । मैंने अपनी
मज़बूरी लिख दी है । अगर मान गए तो ठीक वर्ना वहाँ भी जाना ही पड़ेगा ।”
इसी तरह प्रेमचंद को गांधी का भक्त सिद्ध करने की कोशिश होती रहती है ।
भारतीय राजनीति में गाँधी का आगमन और बोल्शेविक क्रान्ति, दोनों लगभग एक साथ
होते हैं । रूस की बोल्शेविक क्रान्ति और बुल्गारिया की घटनाओं से प्रेमचंद अंजान नहीं हैं ।
प्रेमाश्रम उपन्यास के एक क्रांतिकारी नवयुवक बलराज और गाँव के अन्य किसानों के बीच
अपनी दुर्गति, दशा, नियति, भाग्य आदि पर बहस चल रही होती है । प्रेमचंद बलराज से
कहलवाते हैं - “तुम लोग तो ऐसे हँसी उड़ाते हो मानों काश्तकार कुछ होता ही नहीं । वह
ज़मींदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है; लेकिन मेरे पास जो पत्र आता है, उसमें
लिखा है की रूस देश में काश्तकारों का राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं । उसी के पास कोई
और देश बलगारी (बुल्गारिया) है । वहाँ अभी हाल की बात है, काश्तकारों ने राजा को गद्दी
से उतार दिया है और अब किसानों व मजदूरों की पंचायत काम करती है ।” बोल्शेविक
क्रान्ति से ख़ुश होकर प्रेमचंद लिखते हैं कि ‘मैं धीरे-धीरे बोल्शेविक उसूलों का कायल होता
जा रहा हूँ ।’ परंतु, अपने को गाँधी का चेला कहे जाने पर हँस कर इंकार कर देते हैं । गाँधी
से प्रेमचंद की एकमात्र मुलाक़ात का जिक्र मिलता है । 1935 में नागपुर में हिन्दी साहित्य
सम्मेलन, प्रयाग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था । प्रेमचंद इस अधिवेशन में नागपुर गए थे ।
उन दिनों गाँधी सेवाग्राम (वर्धा) में रह रहे थे । प्रेमचंद ने किसी के माध्यम से यह इच्छा
जाहिर की कि वह गाँधी से मिलना चाहते हैं । गाँधी उन्हें वर्धा बुलाते हैं । छोटी सी
मुलाक़ात होती है । वापस लौट कर प्रेमचंद अपनी पत्नी शिवरानी देवी से इस मुलाक़ात का
ज़िक्र करते हैं । छूटते ही शिवरानी देवी कहती हैं – “अच्छा तो गाँधी का चेला होकर आए
हो’ ? इस पर हँसते हुए प्रेमचंद जवाब देते हैं कि “इसमें चेला होने जैसी क्या बात है । गाँधी
किसानों के लिए, देश के लिए वही लड़ाई अब लड़ रहे हैं जिसे मैं शुरू से अपनी कहानियों
और उपन्यासों में लड़ता रहा हूँ ।” कहना न होगा कि गाँधी द्वारा चलाये जा रहे आंदोलनों
पर प्रेमचंद की नज़र है, वे उनसे प्रभावित भी हैं । इसीलिए, अवध के किसान आंदोलन को
गाँधी का समर्थन न मिलने, बल्कि विरोध करने पर वे कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं ।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे गाँधी से पूरी तरह सहमत हैं, उनके भक्त हो गए हैं ।
प्रेमचंद गाँधी द्वारा हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश के प्रयत्न का स्वागत तो करते हैं लेकिन वह
गाँधी की तरह इसे केवल ‘अछूतों की समस्या’ में सीमित नहीं करते । बल्कि उसे आर्थिक
समस्या के रूप में देखते हैं । उनका मानना है कि केवल मंदिर में अछूतों को प्रवेश मिल जाने
से उनकी जीवन-दशा में सुधार नहीं होने वाला है । उनके कई लेखों और ‘कर्मभूमि’ उपन्यास
में इसे साफ़ तौर पर पढ़ा देखा जा सकता है । इसलिए प्रेमचंद गांधीवादी थे या गाँधी के
भक्त थे, यह साफ़ तौर पर नहीं कहा जा सकता । शहीदे आजम भगत सिंह की फाँसी के
अगले दिन 24 मार्च, 1931 को अपने मित्र दया नारायण निगम को लिखे पत्र में प्रेमचंद
लिखते हैं – “कराची का इरादा था मगर भगत सिंह की फाँसी ने हिम्मत तोड़ दी । अब किस
उम्मीद पर जाऊँ । वहाँ गाँधी का मज़ाक़ उड़ेगा, कांग्रेस ग़ैर ज़िम्मेदार, शोरिशपसंद तबके के
हाथ में आ जाएगी और हम लोगों के लिए उसमें जगह नहीं है । आइंदा क्या तर्ज़े-अमल
अख़्तियार करना पड़े कह नहीं सकता । मगर फ़िलहाल दिल बैठ गया है और मुस्तक़बिल
बिल्कुल तारीक नज़र आता है ।” भगत सिंह की फाँसी के बाद प्रेमचंद कितने दुःखी हैं । उन्हें
अब भारत का मुस्तक़बिल अँधेरा नज़र आता है । गाँधी के सत्याग्रह पर प्रेमचंद की क्या राय
है, उसे भी देखना चाहिए, “किसी प्रोग्राम को उसकी व्यावहारिकता के आधार पर ही
जाँचना उचित है । जिस दिन देश में ऐसे आदमी बड़ी संख्या में निकल आएंगे, जो अपना
सर्वस्व स्वराज्य के लिए त्यागने को तैयार हो जाएँ उस दिन तो आप ही आप स्वराज्य हो
जाएगा । लेकिन ऐसा समय कभी आएगा इसमें संदेह है । ऐसी दशा में सत्याग्रही नीति से
हमें अपने उद्देश्य प्राप्ति की आशा नहीं । सत्याग्रह करके सरकार पर दबाव डालने की
संभावना अब उतनी ही नहीं रही, जितनी दो साल पहले थी । यह मालूम हो गया है कि
सरकार को अगर व्यापार और शासन इन दोनों में से एक लेना पड़े, तो वह शासन को ही
लेगी । व्यापार तो किसी न किसी रूप में शासन से सम्बद्ध किया जा सकता है ।”
जब 15 जनवरी 1334 में बिहार और नेपाल के एक बड़े हिस्से में भयानक भूकंप
आया, जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ तो गाँधी जी ने इस भूकंप को दैवी
कोप मानते हुए इसे वहाँ के लोगों के पापों का फल कहा । इसकी बड़ी आलोचना हुयी । मेरे
देखने में उस समय के दो बड़े भारतीय लेखकों रवीन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद ने इसकी कड़ी
आलोचना की । असल में, गाँधी जी के कार्यक्रमों में धर्म की पवित्रता, नैतिकता, भारतीय
जनमानस में व्याप्त अंधविश्वास को व्यावहारिक कुशलता के साथ तात्कालिक राजनीतिक
परिस्थितियों के लिए किसी भी तर्क से उपयोग में लाए जाने को न तो प्रेमचंद स्वीकार कर
सके न ही टैगोर । बिहार में आए भयंकर भूकंप को लेकर गाँधी जी का अख़बारों में यह
वक्तव्य छपा कि “बिहार का यह अनर्थकारी भूकंप अछूत जातियों के प्रति हो रहे अत्याचारों
और पापकर्मों का ईश्वरीय दंड है ।” गाँधी जी के इस वक्तव्य पर टैगोर, 28 जनवरी 1934
को उन्हें एक पत्र लिखते हैं – “मेरे लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है । लेकिन वास्तव
में आपका यदि यही विचार है तो मेरे विचार से इसका प्रतिरोध होना चाहिए ।” महात्मा
गाँधी ने टैगोर के इस असहमति और प्रतिरोध वाले पत्र को 16 फरवरी 1934 के ‘हरिजन’
में प्रकाशित किया । ‘बिहार का भूकंप’ शीर्षक इस पत्र-लेख में गुरुदेव ने गाँधी के वक्तव्य को
अवैज्ञानिक, विवेकहीन मानते हुए ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं को पाप-पुण्य के नैतिक-अनैतिक
सिद्धांत से जोड़ने वाले एक अंधविश्वासी के रूप में उनकी आलोचना की – “हम लोग जो
महात्माजी की अद्भुत प्रेरक कर्मण्यता के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने देशवासियों के मन
को भय और दुर्बलता से मुक्त किया है और अब उन्हीं लोगों के बीच स्वयं महात्माजी अपने
मुख से अविवेकपूर्ण बातों का महत्व दर्शाते हैं, तो हम गंभीर से आहत महसूस करते हैं ।
अविवेक, जो सभी अंध-शक्तियों का आधार है; जो हमें स्वाधीनता और आत्मसम्मान के
विरुद्ध प्रेरित करता है ।” प्रेमचंद भी 29 जनवरी, 1934 के ‘जागरण’ साप्ताहिक में ‘प्रकृति
का तांडव’ शीर्षक लेख में गाँधी जी का नाम लिए बिना, उनके उक्त विचार का खंडन करते
हैं – “कुछ जो इसे दैवी प्रकोप कहते हैं । क्या दीन, दुःखी, दरिद्र, दलित भारत पर ही दैवी
कोप को आना था ?... साधु कहता है कि लोग साधु-सेवा भूल रहे थे, इसलिए दैवी कोप
आया । वर्णाश्रम संघ शायद यह कहता हो कि मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवाने से कोप
आया । पंडे भी फरमाते हों, देवताओं में लोगों की श्रद्धा कम हो गयी, इसलिए देवता कुपित
हो गए । इसी तरह दफ़्तर के अमले कहते होंगे, लोग अब दिल खोलकर उनकी पूजा नहीं
करते, देते भी हैं तो बहुत रोकर, इसलिए कोप आया । यह सब स्वार्थियों की युक्तियाँ हैं । न
दैवी कोप है न शेषनाग की करवट । यह एक प्राकृतिक विस्फोट है जो वैज्ञानिक कारणों से
आया करता है ।”
अतः प्रेमचंद में जो लोग अंतर्विरोध देखते हैं, उसे उनके युगबोध और युगसीमा दोनों
के साथ देखना उचित होगा । महत्वपूर्ण यह है कि प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या है । दुनिया के
हर बड़े रचनाकार में, यह अंतर्विरोध देखा जा सकता है । वस्तुतः कोई भी यथार्थवादी
लेखक अपने समय में मौजूद सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों-परिस्थितियों की
वास्तविकताओं, सीमाओं व अंतर्विरोधों से बच नहीं सकता । वास्तव में ये अंतर्विरोध
वर्तमान और भविष्य से संवाद और स्वप्न के बीच की द्वंद्वात्मकता को प्रमाणित कराते हैं ।
कई बार इस द्वंद्वात्मकता को ही लेखक का अंतर्विरोध या उसकी द्विविधा (एम्बिबैलेंस) के
रूप में पेश किया जाता है और इसे लेखक की भीरुता अथवा संतुलनवादी समन्वय या
समर्पण में निरसित करने की कोशिश की जाती है । निश्चित तौर पर प्रेमचंद के रचनात्मक
विकास को देखने-समझने के बाद, हर बड़े रचनाकार की तरह उनकी भी सीमाएँ दिखेंगी
और उनमें भी अंतर्विरोध मिलेगा । कहना न होगा कि प्रेमचंद का सम्पूर्ण लेखन उनकी
भावधारा, युगधारा और विचारधारा का सम्मिलित रूप है । औपनिवेशिक आधुनिक भारत
की उपलब्धि और सीमाएँ, उसके अंतर्विरोध प्रेमचंद के यहाँ भी मौजूद हैं, पर प्रेमचंद
दकियानूस, रूढ़िवादी, धर्मांध, प्रतिक्रियावादी ताक़तों, सांप्रदायिकता, सामंती मूल्यों,
जमींदारी शोषण, महाजनी छल-कपट के जीवन भर आलोचक रहे । अपने लेखन में उन्होंने
साहित्य और समाज को प्रगतिशील मूल्यों से ही पोषित और विकसित किए जाने की हमेशा
कोशिश की । प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता को मानव सभ्यता के विकास का बाधक मानते हैं ।
उन्होंने एक तरफ़ हिन्दू संप्रदायवाद के ख़िलाफ़ जमकर लिखा तो वहीं दूसरी तरफ़ मुस्लिम
संप्रदायवाद की भी ख़बर ली है । इस संबंध में उनका प्रसिद्ध लेख ‘सांप्रदायिकता और
संस्कृति’ ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए । ‘गोकुशी’ पर फरवरी 1924 के ‘ज़माना’ में प्रकाशित
उनका लेख ‘मनुष्यता का अकाल’ उन ऋत्विकों और यजमानों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो
लोग प्रेमचंद को भी अपना यजमान बनाने की मुहिम चला रहे हैं । विश्वास करिए उसे
पढ़कर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी । फ़िलहाल ‘सांप्रदायिकता और संस्कृति’
लेख से एक नमूना – सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है । उसे अपने
असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वह गधे की भाँति जो सिंह की
खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर अपना रोब जमाता फिरता था, संस्कृति का खाल
ओढ़कर आती है । हिन्दू अपनी संस्कृति को क़यामत तक सुरक्षित रखना चाहता है,
मुसलमान अपनी संस्कृति को ।...हालाँकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं है ।...फिर
हमारी समझ में नहीं आता, कि वह कौन सी संस्कृति है, जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता
इतना ज़ोर बाँध रही है । वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखंड । और
इसके जन्मदाता भी वही लोग हैं, जो सांप्रदायिकता की शीतल छाया में बैठे विहार कर रहे
हैं । यह सीधे-सादे आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है
और कुछ नहीं ।”
हिन्दी में पहली बार किसानों और मजदूरों के जीवन-मरण की चिंता प्रेमचंद के
साहित्य में मिलती है । तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन में सुराज की उनकी संकल्पना बिना
किसानों और मजदूरों की समस्याओं से मुक्ति के पूरी नहीं होती । वो साफ़ तौर पर कहते हैं
कि ‘स्वराज्य किसानों की माँग है’, वह ‘ग़रीबों का आंदोलन है’ । उनकी इस संकल्पना में
बोल्शेविक क्रान्ति और और विश्व स्तर पर धीरे-धीरे विकसित कम्युनिस्ट आंदोलनों का
प्रभाव था । ‘ज़माना’ उर्दू मासिक पत्र में, फरवरी 1919 को ‘दौरे क़दीम : दौरे जदीद’ (नया
ज़माना : पुराना ज़माना) में वह लिखते हैं – “मगर नए ज़माने ने एक नया पन्ना पलटा है ।
आने वाला ज़माना अब किसानों और मज़दूरों का है । दुनिया की रफ़्तार इसका साफ़ सबूत
दे रही है । हिंदुस्तान इस हवा से बेअसर नहीं रह सकता ।... इंकलाब के पहले कौन जानता
था कि रूस की पीड़ित जनता में इतनी ताक़त छिपी हुई है ।” जर्मन लेखक और फ़िल्म
निर्माता युर्गन रुहेल (Jürgen Rühle) ने अपनी पुस्तक ‘लिट्रेचर एंड रेवोलुशन’ के
एशियाई अध्याय में प्रेमचंद और लु-शुन के उदाहरण से यह दिखाते हैं कि इनके लेखन में
किसानों और मजदूरों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति जो चिंता दिखती है, उसमें एक नए
एशिया का स्वप्न झलकता है । वो लिखते हैं – “भूमि समस्या को जिस तरह से सोवियत संघ
ने सुलझाया है, प्रेमचंद उससे बहुत प्रभावित प्रतीत होते हैं । साधारण एशियाई लोगों के
सरोकारों में यह सबसे प्रमुख समस्या है । प्रेमचंद की अंतिम और सबसे प्रौढ़ रचना ‘गोदान’
हलचलों से भरा एक त्रासद उपन्यास है, जिसमें पूँजीवादी प्रक्रिया के भीतर पिस रहे
किसानों का शोषण चित्रित हुआ है ।”
प्रेमचंद जिस औपनिवेशिक ग़ुलामी को देख रहे थे, किसानों और मजदूरों को दोहरे-
तिहरे शोषण (अंग्रेज़, जमींदार, महाजन) में पिसते हुए देखकर उनके लिए जो सुराज का
सपना देख रहे थे, वह क्या आज भी पूरा हो सका है ? इसलिए जो लोग प्रेमचंद को
ब्राह्मणवाद, सांप्रदायिकता अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने एजेंडे में समाहित करना
चाहते हैं, प्रेमचंद उनके पथ के साथी नहीं हो सकते । प्रेमचंद का रास्ता अलग है । वह सुराज
की क़ीमत पर राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को बहुत महत्व नहीं देते हैं । उनका मानना है
कि “राष्ट्र केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है । वर्तमान राष्ट्र योरोप की इजाद है और राष्ट्रवाद
वर्तमान युग का शाप । पृथ्वी को भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में विभक्त करके उनमें कुछ ऐसी
प्रतियोगिता, ऐसी प्रतिस्पर्द्धा भर दी गयी है कि आज प्रत्येक राष्ट्र की यही कामना है कि
संसार की सारी विभूतियों पर उसी का अधिकार रहे, वही संसार में फलने-फूलने के योग्य है
और किसी राष्ट्र को जीवित रहने का अधिकार नहीं है । एक-दूसरे से इतना सशंक है कि जब
तक अपने को फ़ौलाद से मढ़ न ले, जब तक अपने को गोले-बारूद के अंदर बंद न कर ले, उसे
संतोष नहीं । सब समझते हैं कि सैन्य-व्यय उन्हें मारे डालता है, सब चाहते हैं कि इस
शंकामय प्रवृत्ति का अंत कर दिया जाए । बार-बार इसका उद्योग होता है, सम्मेलन होते हैं
लेकिन सभी चेष्टाएँ निष्फल हो जाती हैं । जब दिलों में सफ़ाई नहीं है तो सम्मेलनों से क्या
होता है ? वहाँ भी हरेक इसी फ़िक्र में रहता है कि नयी-नयी युक्तियों से दूसरे राष्ट्रों को
निरस्त्र करा दे, पर आप अक्षुण्ण बैठा रहे । इसी राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद, व्यवसायवाद आदि
को जन्म देकर संसार में तहलका मचा रखा है ।” वह राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्रीयता
को भी विश्लेषित करते हुए उसे वर्तमान युग का कोढ़ कहते हैं – “राष्ट्रीयता वर्तमान युग का
कोढ़ है, उसी तरह से जैसे मध्य-कालीन युग का कोढ़ सांप्रदायिकता थी । नतीजा दोनों का
एक है । सांप्रदायिकता अपने घेरे के अंदर पूर्ण शांति और सुख का राज्य स्थापित कर देना
चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था, उसको नोचने-खसोटने में उसे ज़रा भी
मानसिक क्लेश न होता था । राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अंदर रामराज्य का
आयोजन करती है । उस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शत्रु है । सारा संसार ऐसे ही राष्ट्रों
या गिरोहों में बंटा हुआ है, और सभी एक दूसरे को हिंसात्मक संदेह की दृष्टि से देखते हैं ।
जब तक इसका अंत न होगा, संसार में शांति का होना असंभव है ।” प्रेमचंद गुरुदेव
रवीन्द्रनाथ टैगोर की तरह राष्ट्रीयता की जगह अंतर्राष्ट्रीयता की हिमायत करते हैं और मानते
हैं कि संसार की जागरूक आत्माएँ इसी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रचार-प्रसार करना चाहती हैं ।
लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर तरह-तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ राष्ट्र उन्हें कल्पनालोक में
विचरने वाला प्राणी अथवा शेखचिल्ली समझता है । प्रेमचंद यहीं नहीं रुकते बल्कि
अंतराष्ट्रीयता की विचारधारा को और साफ़ करते हुए उसे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की आत्मा
कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीयता, एकात्मवाद और समता, इन तीनों को एक दूसरे का पर्याय
मानते हैं । जैसा कि शुरू में ही कहा गया कि यह एकात्मवाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का
‘एकात्मवाद’ नहीं है । प्रेमचंद का रास्ता अलग है । उनका सुराज किसान, मजदूरों और
जनता का सुराज है न कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘धर्मराज्य’ की संप्रभुता वाला
सुराज । प्रेमचंद लिखते हैं – “अंतर्राष्ट्रीयता, एकात्मवाद और समता तीनों मूलतः एक ही हैं ।
उनकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक । आध्यात्मिक मार्ग की
परीक्षा हमने खूब कर ली । कई हज़ार वर्षों से हम यही परीक्षा करते चले आ रहे हैं । वह
श्रेष्ठतम मार्ग था । उसने समाज के लिए ऊँचे से ऊँचे सिद्धान्त की सृष्टि की थी । उसने मनुष्य
की स्वेच्छा पर विश्वास किया, लेकिन फल इसके सिवा और कुछ न हुआ की धर्मोपजीवियों
की एक बहुत बड़ी संख्या पृथ्वी का भार हो गयी । समाज जहाँ था वहीं खड़ा रह गया , नहीं
और पीछे हट गया ।” अतः प्रेमचंद जिस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ थे, आज़ाद भारत का जो
स्वप्न उनके मन में था, वो किसी भी तरह से बंद और संकुचित दृष्टि से पोषित राष्ट्रवाद नहीं
था । ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ तो बिल्कुल नहीं ।
अतः इतिहास को झूठ के वितंडावाद से खारिज़ नहीं किया जा सकता । वह सच के
आईने में अपना अक्स-नक़्श अख़्तियार किए रहता है । प्रगतिशील लेखक संघ से प्रेमचंद के
संबंध को लेकर प्रचारित ‘झूठा-सच’ के बारे में ‘घृणा के प्रचारकों’ को यह जान लेना उचित
होगा कि प्रेमचंद ने न केवल 1936 के अप्रैल महीने में प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) की
सदारत की थी बल्कि हिंदुस्तान में उसके गठन की योजना में भी शामिल रहे । जब 1936
के जनवरी माह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक अहमद अली के
घर पर आयोजित बैठक में प्रगतिशील लेखक संघ के गठन की योजना को अंतिम प्रारूप
दिया जा रहा था प्रेमचंद वहाँ मौजूद थे । प्रेमचंद के अलावा उस बैठक में मेज़बान अहमद
अली, फ़िराक़ साहब, दयानारायण निगम, सदगुरुशरण अवस्थी और सज्जाद ज़हीर मौजूद
थे । उससे पूर्व जनवरी, 1936 के हंस में ‘लंदन में भारतीय साहित्यकारों की एक नयी
संस्था’ शीर्षक लेख में ‘द इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन’ का खुले दिल से इस्तक़बाल
करते हैं और प्रशंसा करते हुए लिखते हैं – “हमें यह जानकार सच्चा आनंद हुआ कि हमारे
सुशिक्षित और विचारशील युवकों में भी साहित्य में भी एक नयी स्फूर्ति और जागृति लाने
की धुन पैदा हो गयी है । लंदन में ‘द इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन’ की इसी उद्देश्य
से बुनियाद डाल दी गयी है और उसने जो अपना मैनिफेस्टो भेजा है, उसे देखकर कर यह
आशा होती है कि अगर यह सभा अपने इस नए मार्ग पर जमी रही तो साहित्य में नवयुग
का उदय होगा । ... हम इस संस्था का हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वह
चिरंजीवी हो ।” वे इस मेनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसका ज़िक्र सज्जाद ज़हीर अपने
लेख ‘प्रगतिशील लेखक संघ पर एक नोट’ (अँग्रेजी से हिन्दी अनुवाद आशुतोष कुमार) में
करते हैं । प्रेमचंद की नज़र में प्रगतिशील होने की परिभाषा हर तरह की संकीर्णता और
सांप्रदायिकता की आलोचना है । ऊपर उद्धृत अपने उसी लेख में प्रेमचंद ‘प्रगतिशीलता’
क्या है उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि “वह सब कुछ जो हमें निष्क्रियता,
अकर्मण्यता और अंधविश्वास की ओर ले जाता है, हेय है । वह सब कुछ जो हममें आलोचना
की मनोवृत्ति लाता है, जो हमें प्रियतम रूढ़ियों को भी बुद्धि की कसौटी पर कसने के लिए
प्रोत्साहित करता है, जो हमें कर्मण्य बनाता है और हममें संगठन की शक्ति लाता है, उसी को
हम प्रगतिशील समझते हैं ।’ इतना ही नहीं अप्रैल, 1936 के हंस में ‘प्रगतिशील लेखक संघ’
नाम से वो एक छोटा सा विज्ञापन भी देते हैं, जिसमें 10 अप्रैल को लखनऊ में होने वाले
सालाना जलसे का जिक्र करते हैं और यह अपील करते हैं कि जिन सज्जनों की संघ के उद्देश्यों
से हमदर्दी हो वह सहभागी बनें – “हमें हर्ष है कि संघ ने उत्साह के साथ काम शुरू कर दिया
है ।...संघ उस साहित्य और कला-प्रवृत्ति का पोशाक है, जो समाज में जागृति और स्फूर्ति
लाए, जो जीवन की यथार्थ समस्याओं पर प्रकाश डाले । संघ ने लखनऊ में 10 अप्रैल को
अपना सालाना जलसा करना निश्चय किया है । जिन सज्जनों को संघ के उद्देश्यों से हमदर्दी
हो, वह श्रीयुत एस. एस. जहीर, ३८ कैनिंग रोड, इलाहाबाद से पत्र-व्यवहार करें ।” चुनांचे
जो लोग इतिहास को झुठलाने में लगे हैं, उनका एजेंडा साफ़ है । किन्तु, प्रेमचंद को अगवा
नहीं किया जा सकता । न ही उनका चन्दन-तिलक संभव है । क्योंकि प्रेमचंद ‘घृणा के
प्रचारकों, और ‘सांप्रदायिक शक्तियों’ के जीवन भर कटु आलोचक रहे । ऐसे में प्रेमचंद और
उनकी परंपरा का हिन्दी-उर्दू लेखन इनकी आँख की किरिकिरी पहले भी बनता रहा है, आज
भी बना हुआ है । पर, हवा की हुक्मरानी से तारीख़ें नहीं बदला करतीं जनाब ! प्रेमचंद का
सम्पूर्ण लेखन आर दृष्टिकोण न पहले, न अभी और न आगे ही इस बात की छूट देता है कि
धर्मांध और सांप्रदायिक ताक़तें उनका चन्दन-तिलक कर, उन्हें तथाकथित रूप से सनातनी
लेखक सिद्ध कर अपने जजमानी की दुकान बढ़ा सकें । क्योंकि प्रेमचंद का साहित्य
फ़िरकापरस्ती, सांप्रदायिकता, धार्मिक भेदभाव और पाखंड, संकीर्ण राष्ट्रवाद, ब्राह्मणवाद-
पुरोहितवाद, आर्थिक ग़ैरबराबरी, ज़मींदारी, सामंतवाद, दलितों, किसानों और मजदूरों के
शोषण के ख़िलाफ़ जाता है । कपास और सूत की मानिंद प्रेमचंद के लेखन में प्रगतिशील
मूल्यों और मानों विन्यस्त हैं । यह सच है कि प्रेमचंद कम्युनिस्ट नहीं थे । पर प्रेमचंद
गांधीवादी भी नहीं थे । वे आर्यसमाज अथवा हिन्दू महासभा के भी मेम्बर नहीं थे । उन्हें हर
उस विचार, धारणा और मत से प्रेम था जिसमें कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड, सांप्रदायिकता,
शोषण, नफ़रत आदि की आलोचना मिलती हो । जिसमें सेक्युलर, ऐहिक और जनपक्षधरता
से लगाव होता । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रख्यात अध्यापक रहे विश्वनाथ
नरवणे ने प्रेमचंद पर एक किताब लिखी है – प्रेमचंद हीज लाइफ एंड वर्क । इस किताब में
नरवणे ने प्रेमचंद के बारे में लिखते हुए कहा है – “प्रेमचंद सेक्युलर थे, रेशनलिस्ट थे, सोशल
जस्टिस को मानने वाले समाजवादी विचारधारा के थे ।” प्रेमचंद पर गांधी के प्रभाव की
बातें तो आपको हर जगह मिल जाएँगी, किन्तु नरवणे ने प्रेमचंद और गाँधी के बीच का फ़र्क़
बताते हुए लिखा है – “तमाम मुद्दों पर गाँधी जी से सहमत होते हुए भी प्रेमचंद और गाँधी
जी में अनेक बातों में भिन्नता दिखाई देती है । अनेक प्रसंगों में गाँधी मध्ययुगीन धारणाओं से
मुक्त नहीं हो पाते, उसके शिकार हो जाते हैं । जबकि प्रेमचंद अपेक्षाकृत आधुनिक और
प्रगतिशील दिखाई देते हैं ।” एक बार मुंशी दया नारायण निगम के यह पूछने पर कि आप
किस राजनीतिक दल के मेंबर हैं, प्रेमचंद का जवाब था कि मैं जिस राजनीतिक पार्टी का
मेम्बर होना चाहता हूँ, वह पार्टी अभी कायम ही नहीं हुयी है । हर बड़े रचनाकार की तरह
प्रेमचंद में भी अंतर्विरोध का होना स्वाभाविक था । प्रेमचंद जिस युगसंधि पर खड़े थे, वह
एक बन रहे, विकसित हो रहे नए युग की दहलीज़ थी । देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि उसी
युगसंधि पर उनके समकालीनों, निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि में यह अंतर्विरोध
किस स्तर पर और कितना था । एक ऐसी तुलना नामवर सिंह अपने एक भाषण/लेख
‘प्रेमचंद के अंतर्विरोध और गांधीवाद’ में करते हैं और कहते हैं कि “हमारे नौजवान
साहित्यकार और लेखक प्रेमचंद के जिन अंतर्विरोधों की चर्चा करना चाहते हैं – ध्यान रखें,
प्रेमचंद अपने युग के उन लेखकों में हैं, जिनमें औरों की तुलना में सबसे कम अंतर्विरोध है ।
ख़ास तौर से प्राचीनता और नवीनता का, मध्ययुगीनता और आधुनिकता का, ऐहिकता और
आनुषंगिकता का ।” अपने इसी वक्तव्य में वो साफ करते हैं कि यह प्रयत्न उचित नहीं कि
‘प्रेमचंद को सोलहों आने मार्क्सवादी साबित किया जाए’ । अतः प्रेमचंद के बारे में कथित
‘नामवर नैरेटिव’ के नाम पर 8 जून के दैनिक जागरण में जिस तरह की अप्रामाणिक,
तथ्यहीन और भ्रामक बातें लिखी गईं, वह अपढ़ आलोचना और पतनशील पत्रकारिता का
नायाब नमूना है । इसीलिए आज जो भी प्रगतिशील मूल्यों को जीने और उसे बचाने की
लड़ाई लड़ रहा है, प्रेमचंद उसके साथ खड़े होंगे, उसकी ताक़त बनेंगे । जो दकियानूस,
प्रतिगामी, सांप्रदायिक मूल्यों को जीने और पोषित-संरक्षित करने वाली ताक़तें हैं, अव्वल तो
प्रेमचंद उनके गले से नीचे नहीं उतरेंगे । मगर किसी सूरमा ने ऐसी हिम्मत की भी तो उसका
‘संस्कार’ हो जाएगा । प्रेमचंद के लेखन में वह शक्ति है । इसीलिए आप देखेंगे कि प्रेमचंद को
बिना पढ़े-समझे, उनके बारे में अनर्गल, अनंत प्रलाप किया जा रहा है । एक ख़ास उद्देश्य के
तहत, चन्दन-तिलक करके उनका ‘सांस्कृतिकरण’ करने का भ्रामक नैरेटिव रचा जा रहा है ।
अतः अगर यह सच है कि प्रेमचंद को कथित रूप से किसी वामपंथी नैरेटिव के सपोर्ट की
दरकार नहीं तो उससे भी बड़ा दृढ़ सत्य यह है (और जिसको वे लोग ख़ूब अच्छी तरह से
जानते भी हैं) कि प्रेमचंद किसी भी तरह के दक्षिणपंथी नैरेटिव में कभी भी न तो घटाए जा
सकते हैं और न ही पढ़े-पढ़ाये जा सकते हैं । उनका असल दर्द यही है । जो कि लाइलाज़ है ।
इन ‘घृणा के प्रचारकों’ में एक जो सबसे अच्छी बात होती है वह यह कि वे इस तरह के
लाइलाज़ मर्ज़ का लुत्फ़ अकेले नहीं लेना चाहते, बल्कि वह चाहते हैं कि इससे उनके संघ-
साथियों में सभी का भला हो :
दोस्तों को भी मिले दर्द की दौलत या रब
मेरा अपना ही भला हो मुझे मंज़ूर नहीं ।
अब, हम आप ऐसे लाइलाज़ मर्ज़ का क्या कर सकते हैं । बस दुआ ही कर सकते हैं कि उन्हें
इस लाइलाज मर्ज़ और उसके दर्द से छुटकारा मिल सके । आमीन !
-विनोद तिवारी